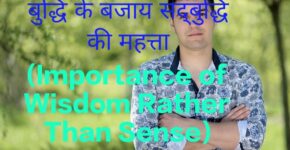Trichotomy of Soul and Mind and Senses
1.अंतरात्मा तथा मन और इंद्रियों की त्रिवेणी (Trichotomy of Soul and Mind and Senses),अन्तरात्मा तथा मन और इंद्रियों का सदुपयोग (Utilization of Conscience and Mind and Senses):
- मानव शरीर अंतरात्मा तथा मन और इंद्रियों की त्रिवेणी (Trichotomy of Soul and Mind and Senses) है अर्थात् संगम है।इसका दुरुपयोग करने पर मानव पशुता से भी नीचे गिर जाता है और सदुपयोग करके देवत्व को प्राप्त कर लेता है।अपने आप को सृष्टि का सबसे सार्थक प्राणी सिद्ध कर सकता है,अतः इन तीनों का संतुलित उपयोग करना चाहिए।
- आपको यह जानकारी रोचक व ज्ञानवर्धक लगे तो अपने मित्रों के साथ इस गणित के आर्टिकल को शेयर करें।यदि आप इस वेबसाइट पर पहली बार आए हैं तो वेबसाइट को फॉलो करें और ईमेल सब्सक्रिप्शन को भी फॉलो करें।जिससे नए आर्टिकल का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।यदि आर्टिकल पसन्द आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर और लाईक करें जिससे वे भी लाभ उठाए।आपकी कोई समस्या हो या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं।इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
Also Read This Article:Control Mind for Success in Exam
2.इंद्रियों का असाधारण उपयोग (Extraordinary use of the senses):
- मानव जीवन का सारा ढांचा इसी प्रयोजन के लिए खड़ा किया गया है।मनुष्य अपने उच्चस्तर से अपनी दुर्बलताओं के कारण ही अधःपतित होता है और दुःख,क्लेश भरा नरक भोगता है।मनुष्य को इस विश्व के साथ संपर्क बनाकर सुखानुभूति प्राप्त करने के तीन उपकरण मिले हुए हैं।यदि वह उनका ठीक तरह उपयोग जान सके तो उसे पग-पग पर यह अनुभव हो कि यह संसार कितना सुंदर और जीवन कितना मधुर है।इन तीन उपकरणों के नाम हैं:अंतरात्मा,मन,इंद्रिय समूह।
- इंद्रियों की बनावट ऐसी अद्भुत है कि दैनिक जीवन की सामान्य प्रक्रिया में ही उन्हें पग-पग पर असाधारण सरसता अनुभव होती है।पेट भरने के लिए भोजन करना स्वाभाविक है।भगवान की कैसी महिमा है कि उसने दैनिक जीवन की शरीर यात्रा भर की नितांत स्वाभाविक प्रक्रिया को कितना सरस बना दिया है।उपयुक्त भोजन करते हुए जीव को कितना रस मिलता है और चित्त को उस अनुभूति से कैसे प्रसन्नता होती है।
- आँख का साधारण काम है वस्तुओं को देखना ताकि हमारी जीवन-यात्रा ठीक तरह चलती रह सके।पर आंखों में कितनी अद्भुत विशेषता भर दी है कि वह रूप,सौंदर्य,कौतुक,कुतूहल जैसी रसभरी अनुभूतियां ग्रहण करके चित्त को प्रफुल्लित बनाती हैं।संसार में उत्पादन,परिपुष्टि,विनाश का क्रम नितांत स्वाभाविक है।मध्यवर्ती स्थिति में हर चीज तरुण होती है और सुंदर लगती है।क्या पुष्प,क्या मनुष्य हर किसी को तीनों स्थितियों में होकर गुजरना पड़ता है।
- मध्यकाल सौंदर्य प्रधान लगता है।वस्तुतः यह तीनों ही स्थितियां अपने क्रम,अपने स्थान और अपने समय पर सुंदर हैं।पर आंखों को सुंदर-असुंदर का भेद करके मध्य स्थित को सुंदर समझने की कुछ अद्भुत विशेषता मिली है।फलस्वरूप जो कुछ उभरता हुआ विकसित,परिपुष्ट दीखता है सो सुंदर लगता है।सुंदर-असुंदर का तात्विक दृष्टि से यहां कुछ भी अस्तित्व नहीं है।पर हमारी अद्भुत आँखें ही हैं जो अपनी सौंदर्यानुभूति वाली विशेषता के कारण हमारे दैनिक जीवन से संबंधित समीपवर्ती वस्तुओं में से सौंदर्य वाला भाग देखतीं,आनंद अनुभव करतीं,उल्लसित और पुलकित होती हैं तथा चित्त को प्रसन्न करती हैं।
- इसी प्रकार जननेंद्रिय की प्रक्रिया है।प्रजनन मक्खी-मच्छरों,कीट-पतंगों,बीज-अंकुरों में भी चलता रहता है।यह सृष्टि का सरल स्वाभाविक क्रम है,पर हमारी जननेंद्रिय में कैसा अजीब उल्लास सरोबार कर दिया है कि संभोग के क्षण ही नहीं-उसकी कल्पना भी मन के कोने-कोने में सिहरन,पुलकन,उमंग और आतुरता भर देती है।तत्त्वतः बात कुछ भी नहीं है।दो शरीरों के दो अवयवों का स्पर्श-इसमें क्या अनोखापन है? क्या अद्भुतता है? क्या उपलब्धि है?
- फिर स्पर्श का कुछ प्रभाव हो भी तो उसकी कल्पना से किस प्रकार,क्यों,किसलिए चित्त को बेचैन करने वाली ललक पैदा होनी चाहिए? बात कुछ भी नहीं है।जननेन्द्रिय की बनावट में एक अद्भुत प्रकार की सरसता का समावेश मात्र है,जो हमें सामान्य स्वाभाविक दांपत्य जीवन के वास्तविक या काल्पनिक,प्रत्यक्ष और परोक्ष क्षेत्रों में एक विचित्र प्रकार की रसानुभूति उत्पन्न करके,जीने भर के लिए प्रयुक्त हो सकने वाले जीवन को निरन्तर उमंगों से भरता रहता है।
- ऊपर जीभ,आंख और जननेन्द्रिय की चर्चा हुई,कान और नाक के बारे में भी इसी प्रकार समझना चाहिए।इंद्रिय समूह अपने साथ रसानुभूति की विलक्षणता इसलिए धारण किए हुए हैं कि सरस,स्वाभाविक,सामान्य जीवन क्रम ऐसे ही नीरस ढर्रे का जीवन भर के लिए मिला हुआ प्रतीत ना हो वरन उसमें हर घड़ी उत्साह,उल्लास,रस,आनंद बना रहे और उसे उपलब्ध करते रहने के लिए जीवन की उपयोगिता,सार्थकता और सरसता का भान होता रहे।इंद्रियसमूह हमें इसी प्रयोजन के लिए उपलब्ध है।यदि उनका उचित,संयमित,विवेकपूर्ण,व्यवस्थापूर्वक उपयोग किया जा सके,तो हमारा भौतिक-सांसारिक जीवन पग-पग पर सरसता,आनंद उपलब्ध करता रह सकता है।
3.मन का सदुपयोग (Utilization of the mind):
- दूसरा उपकरण मन इसलिए मिला है कि संसार में जो कुछ चेतन है,उसके साथ अपनी चेतना का स्पर्श करके और भी ऊंचे स्तर की आनंदानुभूति प्राप्त करे।इन्द्रियाँ जड़ शरीर से संबंधित हैं।जड़ पदार्थों को स्पर्श करके उस संसर्ग का सुख लूटती है।जड़ का जड़ से स्पर्श भी कितना सुखद हो सकता है,इस विचित्रता का अनुभव हमें इंद्रियों के माध्यम से होता है।चेतन का चेतन के साथ,जीवधारी का जीवधारी के साथ स्पर्श-संपर्क होने से मित्रता,ममता,मोह,स्नेह,सद्भाव,घनिष्टता,दया,करुणा,मुदिता जैसी अनुभूतियां होती हैं।
- प्रतिकूल परिस्थितियों में द्वेष,घृणा जैसे भाव भी उत्पन्न होते हैं,पर उनका अस्तित्व है इसीलिए कि मित्रता के वातावरण में संपर्क,संसर्ग का आनंद बिखरता रहे यदि अंधकार ना हो तो प्रकाश की विशेषता नष्ट हो जाय।वस्तुतः मन की बनावट दूसरों के संपर्क,सहयोग,स्नेहभावों के आदान-प्रदान का सुख प्राप्त करने में है।मेले-ठेलों में,सभा-सम्मेलनों में जाने की इच्छा इसलिए उठती है।उन जनसंकुल स्थानों से व्यक्तियों की घनिष्टता न सही समीपता का अदृश्य सुख तो अनायास मिलता ही है।
- चूँकि इंद्रियसुख और जन-संपर्क की घनिष्टता में सहायक एक और नया माध्यम सभ्यता के विकास के साथ-साथ बनकर खड़ा हो गया है,इसलिए अब प्रिय वह भी लगने लगा है-इस तीसरे तत्त्व का नाम है-धन,जिसमें स्वभावतः कोई आकर्षण नहीं।इसमें इंद्रियसमूह या मन को पुलकित करने वाली कोई सीधी क्षमता नहीं है।धातु के सिक्के या कागज के टुकड़े भला आदमी के लिए प्रत्यक्षतः क्यों आकर्षक हो सकते हैं? पर चूँकि वर्तमान समाज व्यवस्था के अनुसार धन के द्वारा इंद्रियसुख के साधन प्राप्त होते हैं,मैत्री संभव होती है,इसलिए धन भी प्रकारान्तर रूप से मन का प्रिय विषय बन गया।अस्तु,धन की गणना भी सुखदायक माध्यमों से जोड़ ली गई है।
- इन तीन शरीरों को जीवात्मा धारण किए हुए है।तीनों की तीन रसानुभूतियाँ हैं।ऊपर दो की चर्चा हो चुकी।स्थूल शरीर की सरसता-इंद्रियसमूह के साथ जुड़ी हुई है।आहार,निद्रा,भय,मैथुन जैसे सुख इंद्रियों द्वारा ही मिलते हैं।
- सूक्ष्म शरीर का प्रतीक मन है।मन की सरसता मैत्री पर,जनसंपर्क पर अवलंबित है।परिवार मोह से लेकर समाज-संबंध,नेतृत्व,सम्मिलन,उत्सव-आयोजन जैसे संपर्कपरक अवसर मन को सुख देते हैं।घटित होने वाली घटनाओं को अपने ऊपर घटित होने की सूक्ष्म संवेदना उत्पन्न करके वह समाज की अनेक हलचलों से भी अपने को बाँध लेता है और उन घटनाक्रमों में खट्टी-मीठी अनुभूतियां उपलब्ध करता है।उपन्यास,सिनेमा,अखबार,रेडियो,इंटरनेट,सोशल मीडिया आदि मन को इसी आधार पर आकर्षित करते और प्रिय लगते हैं।
4.अंतरात्मा की शक्ति का उपयोग और दुरुपयोग (Use and abuse of power of conscience):
- तीसरा रसानुभूति उपकरण है-अंतरात्मा।उसका कार्यक्षेत्र कारण शरीर है।उसमें उत्कृष्टता,उत्कर्ष,प्रगति,गौरव की प्रवृत्ति रहती है,जो उच्च भावनाओं के माध्यम से चरितार्थ होती है।मनुष्य की श्रेष्ठता और सन्मार्गगामिता प्रखर होती रहे,इसके लिए उसमें भी एक रसायानुभूति विद्यमान है-उसका नाम है वर्चस्व,यश,कामना,नेतृत्व,गौरव-प्रदर्शन।उस आकांक्षा से प्रेरित होकर मनुष्य अगणित प्रकार की सफलताएं प्राप्त करता है,ताकि वह स्वयं दूसरों की तुलना में अपने आप को श्रेष्ठ,पुरुषार्थी,पराक्रमी,बुद्धिमान अनुभव करके सुख प्राप्त करे और दूसरे लोग भी उसकी विशेषताओं,विभूतियों से प्रभावित होकर उसे यश,मान प्रदान करें।
- संक्षेप में यह मनुष्य के तीन शरीरों की तीन रसायनुभूतियों की चर्चा हुई।हमारी अगणित योजनाएं,इच्छा,आकांक्षाएं-गतिविधियाँ इन्हीं तीन मूल प्रवृत्तियों के इर्द-गिर्द घूमती हैं।
- भूल मनुष्य की तब होती है,जब वह इन तीनों रसायनुभूतियों को अमर्यादित होकर-अनावश्यक मात्रा में अतिशीघ्र,बिना उचित मूल्य चुकाये प्राप्त करने के लिए आकुल-आतुर हो उठता है और लूट-खसोट की मनोवृत्ति अपनाकर अवांछनीय गतिविधियां अपना लेता है।विग्रह इसी से उत्पन्न होता है।पाप का कारण यही उतावली है।जीवन में अव्यवस्था और अस्तव्यस्तता इसी से उत्पन्न होती है।पतन इसी भूल का परिणाम है।
- अपराधी,दुष्ट और घृणित बनने का कारण उन उपलब्धियों के लिए अनुचित मार्ग को अपनाना ही है।उतावला व्यक्ति आतुरता में विवेक खो बैठता है और औचित्य को भूलकर बहुत जल्दी-अधिक मात्रा में उपर्युक्त सुखों को पाने के लिए असंतुष्ट होकर एक प्रकार से उच्छृंखल हो उठता है।यह अमर्यादित स्थिति उसके लिए विपत्ति बनकर सामने आती है।सरल-स्वभाविक रीति से जो शांतिपूर्वक मिल रहा था-मिलता रह सकता था,वह भी हाथ से चला जाता है और शारीरिक रोग,मानसिक उद्वेग,सामाजिक तिरस्कार,आर्थिक अभाव आत्मिक शांति के संकटों से घिरा हुआ नरक बन जाता है।
- अधिक के लिए उतावला मनुष्य सरल-स्वाभाविक को भी खोकर उल्टा शोक-संताप,कष्ट-क्लेश एवं अभाव-दारिद्रय में फंस जाता है।आमतौर से मनुष्य यह भूल करते हैं।इसी भूल को माया,अज्ञान,अविद्या नामों से पुकारते हैं।यह भूल ही भगवदप्रदत्त पग-पग पर मिलती रहने वाली सरसता से वंचित करती है और इसी के कारण जीव ऊंचा उठने के स्थान पर नीचे गिरता है।
- आत्मज्ञान (अपने आपको जानना,अपनी शक्तियों को जानना) का उद्देश्य मनुष्य के चिंतन और कर्तृत्व को अमर्यादित न होने देने,अवांछनीयता न अपनाने के लिए आवश्यक विवेक और साहस उत्पन्न करना है।मनुष्य अपने अस्तित्व को,लक्ष्य को,व्यवहार को सही तरह समझे।सही मार्ग को अपनाकर सही परिणाम उपलब्ध करते हुए,प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता चले।अपूर्णता से पूर्णता में विकसित हो।यही मार्गदर्शन करना-इसका व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करना आत्मज्ञान का मूल प्रयोजन है।
- स्थूल शरीर का ठीक तरह उपयोग कैसे किया जाए? इंद्रियसमूह को व्यवस्थित और संतुलित कैसे रखा जाय? पारस्परिक संबंधों में औचित्य की,मर्यादा की रक्षा करते हुए अधिकाधिक स्नेह-सद्भाव कैसे प्राप्त किया जाय? आत्मोत्कर्ष की प्रगति और श्रेष्ठता की स्थिति कैसे प्राप्त हो? इन सभी प्रश्नों का समाधान ढूंढने के लिए आत्मविज्ञान की ही सहायता लेनी पड़ती है।अंतरात्मा,मन और इन्द्रियों का प्रयोजन और उपयोग इसी विज्ञान के आधार पर जाना जा सकता है।
- सांसारिक वस्तुओं का समुचित उपयोग कर सकने की जितनी अधिक और जितनी सही जानकारी होगी,उतनी भौतिक जीवन में सुविधा होगी पर जो जितना अनजान होगा वह उतना ही अभावग्रस्त,आपत्तिग्रस्त और असफल रहेगा।ठीक इसी प्रकार सुखी,संतुष्ट और समुन्नत जीवन जीने के लिए आत्मविज्ञान की सही जानकारी का होना आवश्यक है।इसके बिना हमारा चेतन तत्व खिन्न,पतित और दुर्गति की स्थिति में ही पड़ा रहेगा।
5.विद्यार्थी त्रिवेणी का सदुपयोग करें (Students should make good use of Triveni):
- उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो गया होगा कि हम अपनी उन्नति व पतन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं।दूसरा व्यक्ति हमारे पतन का कारण निमित्त कारण तो हो सकता है,मूल कारण नहीं हो सकता है।मूल कारण हमारे कर्म,हमारे विचार,हमारी भावनाएं,हमारे संस्कार,हमारी मनोवृत्ति,हमारी आदतें,हमारा स्वभाव ही उत्थान और पतन के कारण होते हैं।विद्यार्थी काल ऐसा समय होता है जिसमें इन तीनों की शक्तियों को पहचान कर अपनी प्रतिभा,योग्यता,क्षमता को विकसित करने में लगाएँ।
- अक्सर विद्यार्थियों को सही दिशा,सही मार्गदर्शन,सही शिक्षा नहीं मिल पाने के कारण वे इंद्रियों,मन,बुद्धि,आत्मिक शक्ति के बारे में अनजान बने रहते हैं।जब हम इनके बारे में जानेंगे नहीं तो इनका उपयोग,इनको सही दिशा में लगाने,इनका संतुलित उपयोग करने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते हैं।
- यही कारण है कि विद्यार्थियों को गलत संग-साथ मिल जाता है तो उनके देखा-देखी वे भटक जाते हैं और पतन का मार्ग अपना लेते हैं।गलत रास्ता अपनाने वालों का ग्रुप रहता है,इसलिए उन्हें गलत रास्ते पर जाने का एहसास नहीं रहता है।वे सोचते हैं कि और छात्र-छात्राएं भी ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करना सही ही है।हालांकि हमारी अंतरात्मा हमें संकेत करती है और गलत कार्य करते समय भय,शंका,लज्जा का अनुभव होता है परंतु हम बाहरी संगी-साथियों के दाब-दबाव,हमारी वृत्ति बहिर्मुखी होने के कारण हम इस आवाज की अनसुनी कर देते हैं।
- अब स्कूल-कॉलेजों व शिक्षा-संस्थानों में पहले जैसे समर्पित,तपोनिष्ठ गुरु तो हैं नहीं जो आपको सही दिशा,मार्गदर्शन देते हों।आजकल अधिकांश शिक्षक स्वयं ही गलत रास्ते पर चलते हुए मिल जाएंगे अतः उनसे सही दिशा व मार्गदर्शन की अपेक्षा रेत में तेल निकालने के समान है।आजकल के शिक्षकों में विरले ही मिलेंगे जो गुरु जैसे सद्गुण रखते हैं।
- कई बार छात्र-छात्राएं सही रास्ते पर चलते हुए भी अति करने लगते हैं।किसी भी मामले में अति करना उचित नहीं होता है।केवल विद्या,ज्ञान,भक्ति में अति नहीं होती है,क्योंकि ये अनंत है।अब अति कैसे करते हैं,इसे समझ लीजिए।जैसे आपको अध्ययन करने में आनंद आ रहा है।आप जेईई-मेन अथवा अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।आप समय प्रबंधन,उचित रणनीति अपनाए बगैर रात-दिन पढ़ने में जुटे रहेंगे अर्थात् शरीर व इंद्रियों को विश्राम नहीं देंगे तो क्या होगा? यह ठीक बात है कि इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।परंतु आप अपनी क्षमता से अधिक कड़ी मेहनत करेंगे,शरीर को आराम नहीं देंगे,विश्राम नहीं करेंगे,पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं।
- अच्छी चीज को भी अति की सीमा की ओर ले जाने पर वह किसी न किसी प्रकार हमारा नुकसान ही करती है।आप इन उदाहरणों से समझ लीजिए:अत्यधिक अहंकार के कारण रावण जैसे महाविद्वान के कुल का नाश हो गया,अत्यधिक दान देने के कारण बलि को बंधन में बंधना पड़ा,अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता का हरण हुआ।अतः शरीर,मन,बुद्धि,इंद्रियों तथा आत्मिक शक्ति का संतुलित उपयोग करना चाहिए।किसी भी एक चीज की अनदेखी करेंगे और किसी दूसरी चीज का विकास करने में अति करेंगे तो इसके दुष्परिणाम भोगने ही होंगे,आज नहीं तो कल,पर भोगने अवश्य पड़ेंगे क्योंकि कई बार अति करने के परिणाम तत्काल नहीं मिलते हैं।
- उपर्युक्त आर्टिकल में अंतरात्मा तथा मन और इंद्रियों की त्रिवेणी (Trichotomy of Soul and Mind and Senses),अन्तरात्मा तथा मन और इंद्रियों का सदुपयोग (Utilization of Conscience and Mind and Senses) के बारे में बताया गया है।
Also Read This Article:How to Follow Pratyahara Part of Yoga?
6.पुस्तक की चोरी (हास्य-व्यंग्य) (Book Theft) (Humour-Satire):
- दुकानदार (विद्यार्थी से):ऐ लड़के! पुस्तक चुरा रहा है?
- विद्यार्थी:नहीं मैं तो नीचे गिरी हुई पुस्तक को वापस काउंटर पर रखने की कोशिश कर रहा था।
7.अंतरात्मा तथा मन और इंद्रियों की त्रिवेणी (Frequently Asked Questions Related to Trichotomy of Soul and Mind and Senses),अन्तरात्मा तथा मन और इंद्रियों का सदुपयोग (Utilization of Conscience and Mind and Senses) से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न:1.विकासशील व्यक्तित्व का महान गुण क्या है? (What is the great trait of a developing personality?):
उत्तर:हम अपनी सम्मति प्रकट करते समय केवल सत्य और न्याय को देखकर चलें किसी के आदर-तिरस्कार की हमें परवाह न हो।हम केवल अपने आत्म-विकास और आत्म-संतुलन पर दृष्टि रखें।मनुष्यों के समाज में,देवताओं की सभा में,राक्षसों के संग्राम में भी हम अपनी स्वतंत्रता और स्वतंत्र व्यक्तित्व के लिए दृढ़ और संघर्षशील रहें।यदि किसी सत्य को सारा संसार असत्य घोषित करता हो,तो भी हम जन-समुदाय की चिंता ना कर सत्य को सत्य और असत्य को असत्य ही कहें।परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम औरों की सम्मति का सम्मान न करें।उचित परामर्श और सुझाव भले ही वे किसी शत्रु अथवा विपक्षी के द्वारा ही क्यों न दिए गए हों,उन्हें सम्मानपूर्वक अपनाना विकासशील व्यक्तित्व का एक महान गुण है।
प्रश्न:2.उत्कृष्ट व्यक्तित्व की क्या पहचान है? (What is the hallmark of an outstanding personality?):
उत्तर:अपने मन,बुद्धि,मन और बुद्धि के आवेगों के आवेश और मनोवृत्तियों की चंचलता को भंग ना होने दें।प्रत्येक निर्णय गुण-दोष देखकर,सत्य-असत्य को ध्यान में रखकर;विवेक की कसौटी पर कसकर ही करें।हर एक के अच्छे-से-अच्छे स्वरूप को ढूंढ निकालने की यथाशक्ति चेष्टा ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की पहचान है।
प्रश्न:3.गलत रास्ते पर भटकने का मूल कारण क्या है? (What is the root cause of straying on the wrong path?):
उत्तर:अज्ञान,बुरी संगत,हमारी बुरी आदतें और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण भटक जाते हैं।
- उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर द्वारा अंतरात्मा तथा मन और इंद्रियों की त्रिवेणी (Trichotomy of Soul and Mind and Senses),अन्तरात्मा तथा मन और इंद्रियों का सदुपयोग (Utilization of Conscience and Mind and Senses) के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
| No. | Social Media | Url |
|---|---|---|
| 1. | click here | |
| 2. | you tube | click here |
| 3. | click here | |
| 4. | click here | |
| 5. | Facebook Page | click here |
| 6. | click here |
Related Posts
About Author
Satyam
About my self I am owner of Mathematics Satyam website.I am satya narain kumawat from manoharpur district-jaipur (Rajasthan) India pin code-303104.My qualification -B.SC. B.ed. I have read about m.sc. books,psychology,philosophy,spiritual, vedic,religious,yoga,health and different many knowledgeable books.I have about 15 years teaching experience upto M.sc. ,M.com.,English and science.